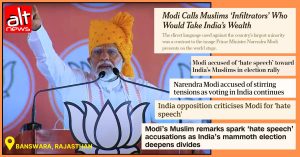किसानों के हाल के प्रदर्शन से जोड़कर कई पुराने और असंबंधित वीडियोज़ और तस्वीरें शेयर की गई हैं. इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए खालिस्तान के नारे और पाकिस्तान के झंडे वाला ब्रिटेन का एक पुराना वीडियो इस प्रदर्शन से जोड़कर शेयर किया गया था. इसके अलावा, खालिस्तान के समर्थन में पोस्टर लिए खड़े एक व्यक्ति की 7 साल पुरानी तस्वीर किसान आन्दोलन से जोड़कर की शेयर की गयी. इस बीच, सोशल मीडिया पर नीले रंग के कपड़े और पगड़ी पहने कुछ लोगों के जुलूस का वीडियो वायरल है. यूज़र्स ये वीडियो शेयर करते हुए किसान आंदोलन और खालिस्तान मूवमेंट के बीच कनेक्शन होने की बात कह रहे हैं. ध्यान दें कि वीडियो के साथ लिखे गए मेसेज में इसे हाल का नहीं बताया गया है.
ट्विटर यूज़र ‘आकाश आरएसएस’ ने भी ऐसे ही दावों के साथ ये वीडियो ट्वीट किया. आर्टिकल लिखे जाने तक इस वीडियो को 20 हज़ार बार देखा जा चुका है. पहले भी इस यूज़र को कई बार सोशल मीडिया पर गलत जानकारियां शेयर करते हुए पाया गया है. (ट्वीट का आर्काइव लिंक)
इस वीडियो को देखकर आपको समझ आ जायेगा कि किसान आंदोलन और खालिस्तान मूवमेंट में क्या कनेक्शन है और ये आंदोलन कहाँ से संचालित हो रहा है pic.twitter.com/EipzjFdS97
— Akash RSS (@Satynistha) December 3, 2020
ट्विटर हैन्डल ‘@SonuSri795’ ने भी ये वीडियो इसी दावे के साथ ट्वीट किया है. (ट्वीट का आर्काइव लिंक)
इस वीडियो को देखकर आपको समझ आ जायेगा कि किसान आंदोलन और खालिस्तान मूवमेंट में क्या कनेक्शन है और ये आंदोलन कहाँ से संचालित हो रहा है pic.twitter.com/Md5pwTht9t
— सुधीर श्रीवास्तव उर्फ सोनू (@SonuSri795) December 4, 2020
एक और ट्विटर यूज़र ने भी ये वीडियो ट्वीट किया है. (ट्वीट का आर्काइव लिंक)
इस वीडियो को देखकर आपको समझ आ जायेगा कि किसान आंदोलन और खालिस्तान मूवमेंट में क्या कनेक्शन है और ये आंदोलन कहाँ से संचालित हो रहा है। pic.twitter.com/RMpUv8Lj5F
— Ankur Agarwal (@aannkuur_) December 4, 2020
फ़ैक्ट-चेक
की-वर्ड्स सर्च करने पर हमें ये वीडियो 22 जून 2018 को पोस्ट किया हुआ मिला. शुभ पंडित नाम के यूज़र ने ये वीडियो पोस्ट किया था. इसके अलावा, 26 जून 2018 को फ़ेसबुक यूज़र हिमांशु शुक्ला ने भी ये वीडियो पोस्ट किया था.
पंजाबी की-वर्ड्स से सर्च करने पर हमें फ़ेसबुक यूज़र हरदीप सिंह खालसा द्वारा बेहतर क्वालिटी में शेयर किया हुआ ये वीडियो मिला. इस वीडियो में 15 सेकंड पर नीले रंग की टी-शर्ट पर सैन फ़्रांसिस्को लिखा हुआ है.

इस वीडियो में प्रॉपर होटल नाम का एक बोर्ड दिखाई देता है. इसके चलते हमने गूगल मैप पर प्रॉपर होटल सर्च किया. ऑल्ट न्यूज़ ने पाया कि ये वीडियो इसी जगह पर रिकॉर्ड किया गया था.
इसके अलावा, वीडियो में दिख रही काली रंग की इमारत, जिस पर ‘Charmaine’s’ लिखा हुआ है, दरअसल एक रेस्टोरेंट है. लाइव लोकेशन देखते हुए हमें वीडियो में दिखने वाली इमारत गूगल मैप पर मिली.
गूगल पर मौजूद तस्वीरों की तुलना वायरल हो रहे वीडियो के फ़्रेम्स से तुलना करने पर ये बात साफ़ हो जाती है.


कुल मिलाकर, सैन फ़्रांसिस्को में खालिस्तान मूवमेंट के समर्थन में हुई रैली का वीडियो हाल के किसान प्रदर्शन से जोड़कर शेयर किया गया.
मुस्लिम लड़की की 2012 की तस्वीर एडिट कर ग़लत मेसेजेज़ के साथ किया जा रहा है शेयर:
सत्ता को आईना दिखाने वाली पत्रकारिता का कॉरपोरेट और राजनीति, दोनों के नियंत्रण से मुक्त होना बुनियादी ज़रूरत है. और ये तभी संभव है जब जनता ऐसी पत्रकारिता का हर मोड़ पर साथ दे. फ़ेक न्यूज़ और ग़लत जानकारियों के खिलाफ़ इस लड़ाई में हमारी मदद करें. नीचे दिए गए बटन पर क्लिक कर ऑल्ट न्यूज़ को डोनेट करें.
बैंक ट्रांसफ़र / चेक / DD के माध्यम से डोनेट करने सम्बंधित जानकारी के लिए यहां क्लिक करें.